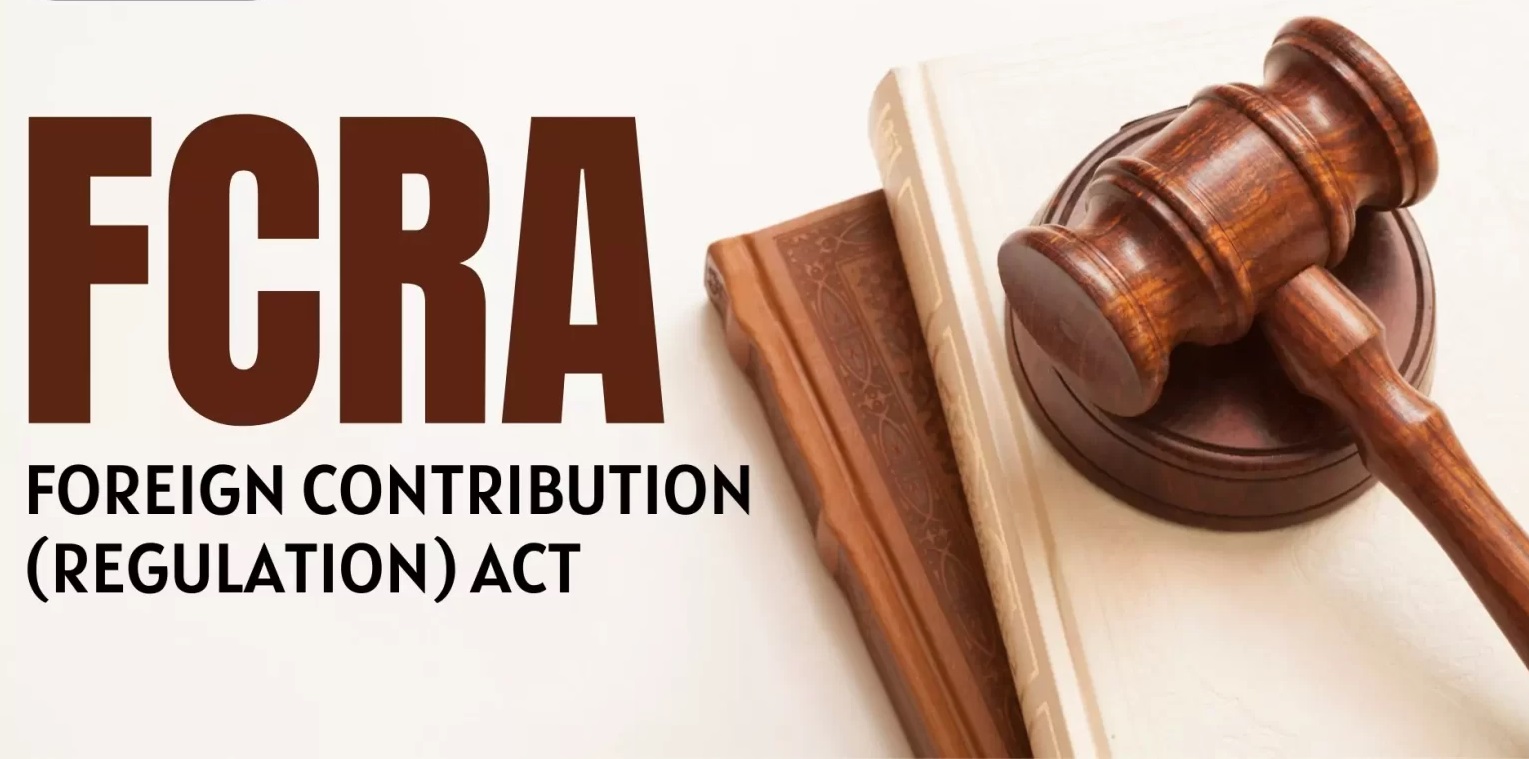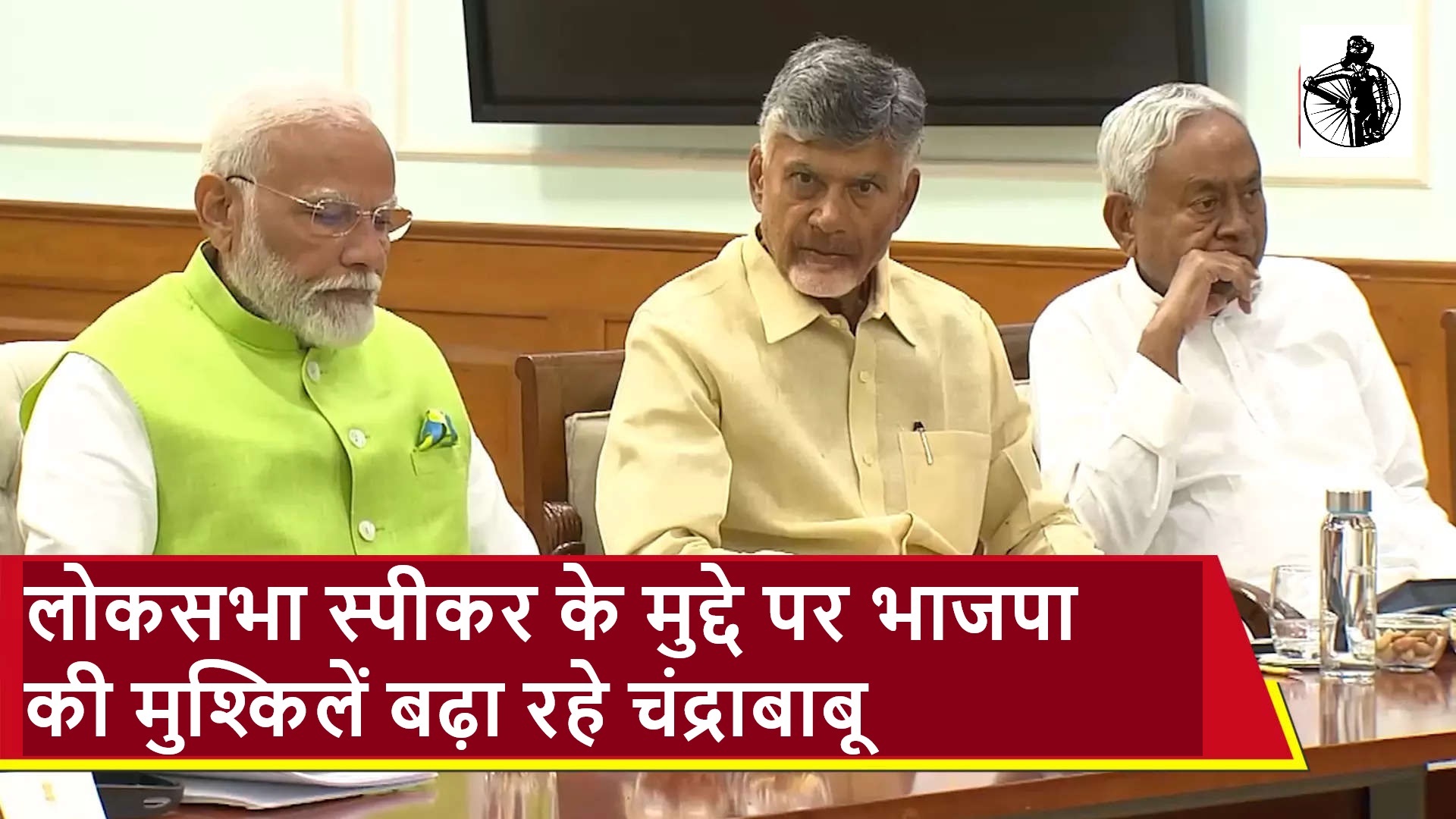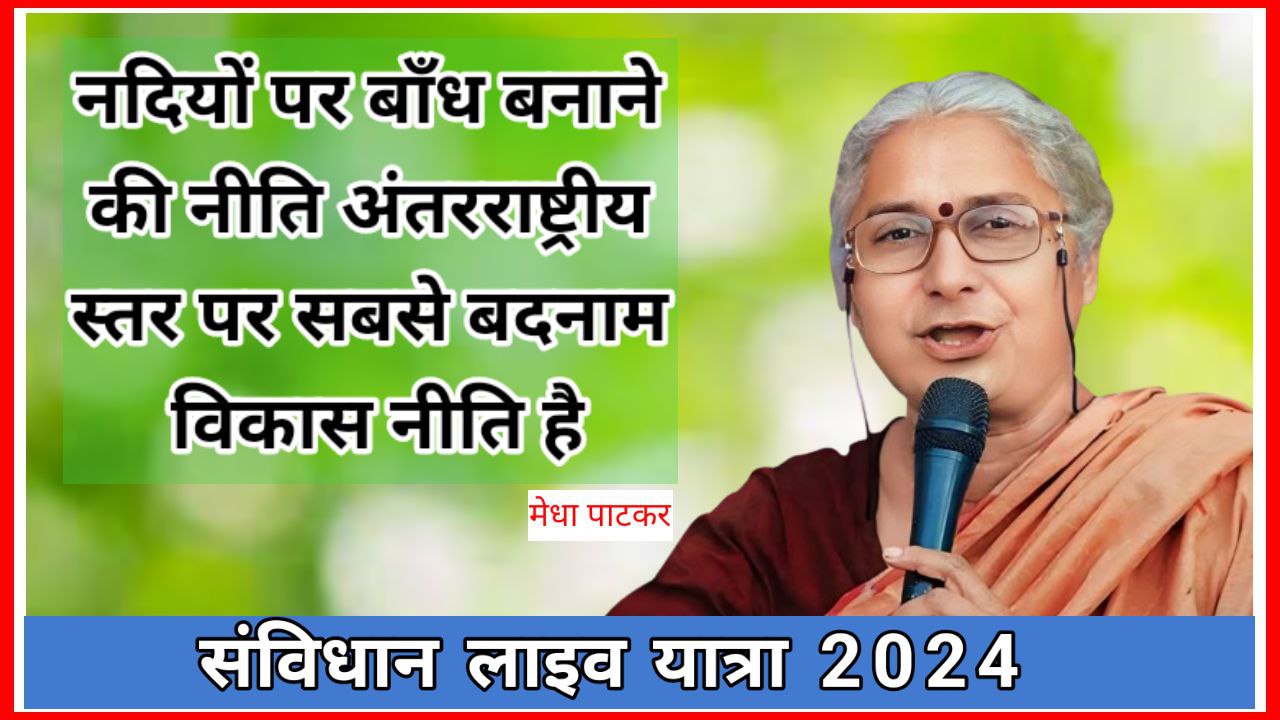भक्ति आन्दोलन: भारतीय जीवन दर्शन की विविधता में ध्येयपूर्ण जीवन को संगति देता काव्य काल
सचिन श्रीवास्तव
मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आन्दोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस दौर में सामाजिक-धार्मिक सुधारकों ने समाज में विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार-प्रसार किया। सिख धर्म के उद्भव में भी भक्ति आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। पूर्व मध्यकाल में जिस भक्ति धारा ने अपने आन्दोलनात्मक सामर्थ्य से पूरे देश को नए सिरे से झकझोरा था। इसकी शुरुआत के कारणों पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन इस बात पर सभी की सहमति है कि भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में छठवीं-सातवीं शताब्दी में ही शुरू हो गई थी। 14वीं शताब्दी तक आते-आते इसने उत्तर भारत में आन्दोलन का रूप ग्रहण कर लिया। लेकिन यह धारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत कैसे आई, उसके आन्दोलनात्मक रूप धारण करने के कौन से कारण रहे, इस पर पर्याप्त मतभेद हैं। अब तो बहुत से आलोचक भक्ति आन्दोलन से संबंधित 19वीं-20वीं शताब्दी के विचारों पर प्रश्न उठाने लगे हैं। अनेक विद्वान अब मध्य युग के भक्ति आन्दोलन को वैदिक परम्परा की मूल बातों का नए रूप में उदय के रूप में देखने लगे हैं।
भक्ति के उद्भव एवं विकास के समय जो कुछ भी भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति तथा इतिहास को प्राप्त हुआ, वह स्वयं में अद्भुत, अनुपम एवं दुर्लभ है। अन्ततः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में कह सकते है –
समूचे भारतीय इतिहास में यह अपने तरह का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। भक्ति का यह नया इतिहास मनुष्य जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यह लक्ष्य है भगवद्भक्ति, आदर्श है शुद्ध सात्विक जीवन और साधन है भगवान के निर्मल चरित्र और सरस लीलाओं का गान।
भक्ति आंदोलन की शुरुआत
भक्ति आन्दोलन का आरम्भ दक्षिण भारत में आलवारों एवं नायनारों से हुआ जो कालान्तर में 800 ईसवी से 1700 ईसवी के बीच उत्तर भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में फैल गया। इस क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे जो हिंदू मत के एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे हैं। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता दी।
इस अभियान की प्रमुख उपलब्धि तो यही थी कि इस दौर में मूर्ति पूजा लगभग समाप्त हो गई थी।
भक्ति आंदोलन के नेता रामानन्द ने राम को भगवान के रूप में लेकर इसे केंद्रित किया। उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे 15वीं शताब्दी की शुरुआत में रहे। उन्होंने सिखाया कि भगवान राम सर्वोच्च भगवान हैं और केवल उनके प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से और उनके नाम को बार-बार उच्चारित करने से ही मुक्ति पाई जाती है।
चैतन्य महाप्रभु सोलहवीं शताब्दी के दौरान बंगाल में हुए। भगवान के प्रति प्रेम भाव रखने के प्रबल समर्थक, भक्ति योग के प्रवर्तक, चैतन्य ने ईश्वर की आराधना श्रीकृष्ण के रूप में की।
इसी दौर में श्री रामानुजाचार्य, जो भारतीय दर्शनशास्त्री थे। उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैष्णव संत के रूप में मान्यता दी गई है। रामानंद ने उत्तर भारत में जो किया वही रामानुज ने दक्षिण भारत में किया। उन्होंने रुढिवादी विचारों की बढ़ती औपचारिकता के खिलाफ आवाज उठाई और प्रेम और समर्पण की नींव पर आधारित वैष्णव विचाराधारा के नए संप्रदाय की स्थापना की। उनका सबसे बड़ा योगदान अपने मानने वालों के बीच जाति के भेदभाव को समाप्त करना था।
बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में भक्ति आन्दोलन के अनुयायियों में संत शिरोमणि रविदास, नामदेव और संत कबीर दास शामिल हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के जरिये से भक्ति गीतों पर बल दिया। यह ज्ञान मार्गी शाखा थी।
पहले सिक्ख गुरु और सिक्ख धर्म के प्रवर्तक, गुरु नानक जी भी संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने सभी प्रकार के जाति भेद और धार्मिक शत्रुता और रीति रिवाजों का विरोध किया। उन्होंने ईश्वर को एक रूप माना और हिन्दू और मुस्लिम धर्म की औपचारिकताओं तथा रीति रिवाजों की आलोचना की। गुरु नानक का सिद्धांत सभी लोगों के लिए था। उन्होंने हर प्रकार से समानता का समर्थन किया। सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में भी अनेक धार्मिक सुधारक आए। वैष्णव सम्प्रदाय के राम के अनुयायी और कृष्ण के अनुयायी अनेक छोटे वर्गों और पंथों में बंट गए। राम के अनुयायियों में प्रमुख संत कवि तुलसीदास थे। तुलसीदास अपने दौर के भारतीय दर्शन और साहित्य के सबसे बड़े अध्येताओं में से एक थे। उनकी महान कृति ‘रामचरितमानस’ जिसे आम बोलचाल में हम ‘तुलसी रामायण’ कहते हैं, उसकी लोकप्रियता का कोई जोड़ आज तक नहीं है। उन्होंने लोगों के बीच राम की जो छवि सर्वव्यापी, सर्व शक्तिमान, दुनिया के स्वामी और परब्रह्म के साकार रूप से बनाई, वह छवि आज भी देश के सभी हिस्सों में समान रूप से देखी, मानी जाती है।
कृष्ण के अनुयायियों ने 1585 ईसवी में राधा-बल्लभी पंथ की स्थापना की। सूरदास ने ब्रजभाषा में सूर सागर की रचना की, जो श्री कृष्ण के मोहक रूप और उनकी प्रेमिका राधा की कथाओं से उपजती है।
भक्ति आन्दोलन की विशेषताएं
यह आन्दोलन कम या ज्यादा पूरे दक्षिणी एशिया यानी भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था और यह बेहद लम्बे काल खंड को एक करता है। इसमें समाज के सभी वर्गों (कथित निम्न और उच्च जातियां, स्त्री-पुरुष, सनातनी, सिख, मुसलमान सभी का प्रतिनिधित्व रहा। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप संस्कृत के बजाय क्षेत्रीय भाषाओं में भारी मात्रा में हिन्दू साहित्य की रचना हुई, जो मुख्यतः भक्ति काव्य और संगीत के रूप में है। भक्ति आन्दोलन से हिन्दू समाज ने सत्ता के दुष्प्रचारों, जोर-जबरजस्ती, कड़े कानूनों और दैनिक जीवन में राजनैतिक हस्तक्षेप का कड़ा मुकाबला किया। सूफीवाद के रूप में इसका इस्लाम पर भी प्रभाव पड़ा।
भक्ति आंदोलन के बारे में विविध राय
बालकृष्ण भट्ट के लिए भक्तिकाल की उपयोगिता अनुपयोगिता का प्रश्न मुस्लिम चुनौती का सामना करने से सीधे सीधे जुड़ गया था। इस दृष्टिकोण के कारण भट्ट जी ने मध्यकाल के भक्त कवियों का काफी कठोरता से विरोध किया और उन्हें हिन्दुओं को कमजोर करने का जिम्मेदार भी ठहराया। भक्त कवियों की कविताओं के आधार पर उनके मूल्यांकन के बजाय उनके राजनीतिक सन्दर्भों के आधार पर मूल्यांकन का तरीका अपनाया गया। भट्ट जी ने मीराबाई व सूरदास जैसे महान कवियों पर हिन्दू जाति के पौरुष पराक्रम को कमजोर करने का आरोप मढ़ दिया। उनके मुताबिक समूचा भक्तिकाल मुस्लिम चुनौती के समक्ष हिन्दुओं में मुल्की जोश जगाने में नाकाम रहा। भक्त कवियों के गाये भजनों ने हिन्दुओं के पौरुष और बल को खत्म कर दिया।
रामचन्द्र शुक्ल जी ने भक्ति को पराजित, असफल और निराश मनोवृत्ति की देन माना था। कई अन्य विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया जैसे, बाबू गुलाब राय आदि। डॉ॰ राम कुमार वर्मा का मत भी यही है -: मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले इस मत का खंडन किया और प्राचीनकाल से यानी दूसरी और 5वीं शताब्दी से इस भक्ति धारा का संबंध स्थापित करते हुए अपने मत को स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा – यह बात अत्यन्त उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मन्दिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की धारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिन्ध में, फिर उसे उत्तरभारत में, प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में।
भक्ति आन्दोलन के प्रमुख सन्त
- अलवर (लगभग दूसरी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक; दक्षिण भारत में)
- नयनार (लगभग 5वीं शताब्दी से 10वी शताब्दी तक; दक्षिण भारत में)
- आदि शंकराचार्य (788ई से 820 ई)
- रामानुज (1017 – 1137)
- बासव (12वीं शताब्दी)
- जयदेव (12वीं शताब्दी)
- माधवाचार्य (1238 – 1317)
- नामदेव (1270 – 1309; महाराष्ट्र)
- एकनाथ – गीता पर भाष्य लिखा ; विठोबा के भक्त
- सन्त ज्ञानेश्वर (1275 – 1296; महाराष्ट्र)
- निम्बकाचार्य (13वीं शताब्दी)
- रविदास (1377-1528)
- रामानन्द (15वीं शती)
- पुरन्दर (15वीं शती; कर्नाटक)
- पीपा (जन्म 1425)
- कबीरदास (1440 – 1510)
- शंकरदेव (1449 – 1569 ; असम में)
- चैतन्य महाप्रभु (1468 – 1533; बंगाल में)
- गुरु नानक (1469 – 1538)
- हरिदास (1478 – 1573; महान संगीतकार जिहोने भगवान विष्णु के गुण गाये)
- वल्लभाचार्य (1479 – 1531)
- सूरदास (1483 – 1563; बल्लभाचार्य के शिष्य थे)
- मीराबाई (1498 – 1563; राजस्थान में ; कृष्ण भक्ति)
- तुलसीदास (1532 – 1623)
- दादू दयाल (1544-1603; कबीर के शिष्य थे)
- समर्थ रामदास (शिवाजी के गुरू ; दासबोध के रचयिता)
- तुकाराम (शिवाजी से समकालीन ; विठल के भक्त)
- रामकृष्ण परमहंस (1836 – 1886)
- त्यागराज (मृत्यु 1847)
- भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद (1896 – 1977)
- कवि प्रसाद गौतम ( 1905 – 1885 ; नेपाल )
स्वामी माधवाचार्य (संवत् 1254-1333) ने ‘ब्राह्म संप्रदाय’ नाम से द्वैतवादी वैष्णव सम्प्रदाय चलाया जिसकी ओर लोगों का झुकाव हुआ। इसके साथ ही द्वैताद्वैतवाद (सनकादि सम्प्रदाय) के संस्थापक निम्बार्काचार्य ने विष्णु के दूसरे अवतार कृष्ण की प्रतिष्ठा विष्णु के स्थान पर की और लक्ष्मी के स्थान पर राधा को रख कर देश के पूर्वी भाग में प्रचलित कृष्ण-राधा (जयदेव, विद्यापति) की प्रेम कथाओं को नया रूप दिया। वल्लभाचार्य जी ने भी कृष्ण भक्ति के प्रसार का कार्य किया। सूरदास भी इस सम्प्रदाय की प्रसिद्धि के मुख्य कारण कहे जा सकते हैं। सूरदास ने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेकर कृष्ण की प्रेमलीलाओं एवं बाल क्रीड़ाओं को भक्ति के रंग में रंग कर प्रस्तुत किया।
इस तरह दो मुख्य संप्रदाय सगुण भक्ति के भीतर पूरे उत्कर्ष पर इस काल में विद्यमान थे – रामभक्ति शाखा; कृष्णभक्ति शाखा।
इसके अतिरिक्त भी दो शाखाएं प्रचलित हुईं – प्रेममार्ग (सूफ़ी) और निर्गुणमार्ग शाखा।
सगुण धारा के इस विकास क्रम के समानांतर ही बाहर से आए हुए मुसलमान सूफ़ी संत भी अपने विचारों को सामान्य जनता में फैला रहे थे। मुसलमानों के इस लंबे प्रवास के कारण भारतीय तथा मुस्लिम संस्कृति का आदान-प्रदान होना स्वाभाविक था। फिर इन सूफ़ी संतों ने भी अपने विचारों को जनसाधारण में व्याप्त करने की, अपने मतों को भारतीय आख्यानों में, भारतीय परिवेश में, यहीं की भाषा-शैली लेकर प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया। इनके मतों में कट्टरता का कोई हिस्सा नहीं था। इनका मुख्य सिद्धान्त प्रेम तत्त्व था।
हालांकि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में कुछ अन्तर जरूरत था इसके बावजूद इनके प्रेम तत्त्व को फैलाने की शैली ने लोगों को आकर्षित किया। इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन भी किया जिसे कुछ लोगों ने अद्वैतवाद ही मान लिया, जो कि सही नहीं है।
हज़रत निज़ामुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती आदि अनेक संतों ने हिन्दू-मुसलमान सबका आदर प्राप्त किया। इस सूफ़ी मत में भी चार धाराएं मुख्यत: चलीं-
(1) चिश्ती सम्प्रदाय
(2) कादरी सम्प्रदाय
(3) सुहरावर्दी सम्प्रदाय
(4) नक्शबंदिया सम्प्रदाय।
जायसी, कुतुबन, मंझन आदि प्रसिद्ध (साहित्यकार) कवियों ने हिन्दी साहित्य को अमूल्य साहित्य रत्न भेंट किए। निर्गुणज्ञानाश्रयी शाखा पर भी इनका प्रभाव पड़ा तथा हिन्दू-मुसलमानों के भेद को मिटाने की बातें कही जाने लगीं। आचार्य शुक्ल ने भी इन्हें ’हिन्दू और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाला’ कहा।
रामानन्द जी उत्तर भारत में रामभक्ति को लेकर आए थे। उनके सिद्धान्तों में इस भक्ति का स्वरूप दो प्रकार का था – राम का निर्गुण रूप; राम का अवतारी रूप। ये दोनों मत एक साथ ही थे। निर्गुण रूप में राम का नाम तो होता पर उसे ’दशरथ-सुत’ की कथा से सम्बद्ध नहीं किया जाता। रामानन्द ने देखा कि भगवान की शरण में आने के उपरान्त छूआ-छूत, जाँत-पाँत आदि का कोई बन्धन नहीं रह जाता अत: संस्कृत के पण्डित और उच्च ब्राह्मण कुलोद्भूत होने के पश्चात भी उन्होंने देश-भाषा में कविता लिखी और सबको (ब्राह्मण से लेकर निम्नजाति वालों तक को) राम-नाम का उपदेश दिया। कबीर इन्हीं के शिष्य थे। कबीर, रैदास, धन्ना, सेना, पीपा आदि इनके शिष्यों ने इस मत को प्रसिद्ध किया। रामनाम के मंत्र को लेकर चलने वाले अक्खड़-फक्कड़ संतों ने भेद-भाव भुला कर सबको प्रेमपूर्वक गले लगाने की बात कही। वैदिक कर्मकाण्ड के द्वारा फैले हुए आडंबरों एवं बाह्य विधि-विधानों के त्याग पर बल देते हुए राम नाम का प्रेम, श्रद्धा से स्मरण करने की सरल पद्धति और सहज समाधि का प्रसार किया। कबीर में तीन प्रमुख धाराएँ समाहित दिखाई देती हैं –
(1) उत्तरपूर्व के नाथपंथ और सहजयान का मिश्रित रूप
(2) पश्चिम का सूफ़ी मतवाद और
(3) दक्षिण का वेदान्तभावित वैष्णवधर्म
हठयोग का कुछ प्रभाव इन पर अवश्य है परन्तु मुख्यत: प्रेम तत्त्व पर ही बल दिया गया है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन संतों का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। इन संतों के साहित्य में हमें तत्कालीन युग की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक समस्त स्थितियों के दर्शन हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी इनका योग बहुत है। सहज प्रेम की भाषा पर बल देने के कारण लोगों का इन पर भी बहुत झुकाव रहा। कबीर की मृत्यु के कुछ समय बाद इसमें भी सम्प्रदाय की स्थापना हो गई। अन्य शाखाओं के समान इसका महत्व भी भक्तिकाल को पूर्ण बनाने में है।
ये चारों शाखाएँ भक्तिकाल या मध्यकाल के पूर्व भाग में अपने उत्कर्ष में थीं। इन चारों ही शाखाओं ने हिन्दी साहित्य को बड़े-बड़े व्यक्तित्व प्रदान किए जैसे – सूर, तुलसी, कबीर आदि। अपने भक्तिभाव की चरम उत्कृष्टता के लिए भी ये जनता के मन-मानस पर आधिपत्य कर सके। आज भी ये श्रद्धा एवं आदर से देखे जाते हैं। यद्यपि कालान्तर में इन सम्प्रदायों में भी अनैतिकता के तत्त्वों के प्रवेश के कारण शुद्धता नहीं रह गई थी तथा इनका पतन भी धीरे-धीरे हो गया था तथापि जो अद्भुत मणियाँ इस काल में प्राप्त हुईं, वे किसी भी अन्य काल में प्राप्त नहीं हो सकीं, यह निस्संदेह कहा जा सकता है। भक्तिकाल में हर प्रकार से कला समृद्धि हुई, नवीन वातावरण का जन्म हुआ, जन-जन में भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के स्रोत फूट पड़े, ऐसा काल वस्तुत: साहित्येतिहास का “स्वर्णकाल” कहलाने योग्य है।
सम्प्रदायों से मुक्त रूप में भी भक्ति का प्रचार था। मीरा, रसखान, रहीम का नाम उतनी ही श्रद्धा से लिया जाता है जितना कि किसी सम्प्रदायबद्ध संत कवि का। इस तरह कहा जा सकता है कि जनता में सम्प्रदाय से भी अधिक शुद्ध भक्ति-भाव की महत्ता थी। ऐकान्तिक भक्ति ने समष्टिगत रूप धारण किया और जन-जन के हृदय को आप्लावित कर दिया।
भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारण
- हिन्दू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला।
- सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिन्दुओं को प्रभावित किया; जिस कारण से हिन्दू, इस्लाम के सिद्धांतों के निकट सम्पर्क में आये।
- हिन्दुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊँच-नीच एवं जात-पात का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग व अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिये बोधगम्य नहीं रह गया था।
- मुस्लिम शासकों द्वार मूर्तियों को नष्ट एवं अपवित्र कर देने के कारण, बिना मूर्ति एवं मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा, जिसके लिये उन्हें भक्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ा।
- तत्कालीन भारतीय समाज की शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के कारण निचले वर्णों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भक्ति-संतों द्वारा दिये गए सामाजिक सौहार्द्र और सद्भाव के संदेश ने लोगों को प्रभावित किया।
भक्ति आंदोलन का महत्त्व
- भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने कर्मकांडों से मुक्त जीवन का ऐसा लक्ष्य रखा, जिसमें ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान नहीं था।
- भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल दिया, जिससे इन समुदायों के मध्य सहिष्णुता और सद्भाव की स्थापना हुई।
- भक्तिकालीन संतों ने क्षेत्रीय भाषों की उन्नति में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी, पंजाबी, तेलुगू, कन्नड़, बंगला आदि भाषाओं में इन्होंने अपनी भक्तिपरक रचनाएँ कीं।
- भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति-बंधन की जटिलता कुछ हद तक समाप्त हुई। फलस्वरूप दलित व निम्न वर्ग के लोगों में भी आत्मसम्मान की भावना जागी।
- भक्तिकालीन आंदोलन ने कर्मकांड रहित समतामूलक समाज की स्थपाना के लिये आधार तैयार किया।
- भक्ति आंदोलन से हिन्दू-मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। भक्तिमार्गी संतों ने समता का प्रचार किया और सभी धर्मों के लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिये प्रयास किये।
भक्ति काल और रीतिकाल के बीच का दौर
तुलसी की मृत्यु (1680 ई.) के कुछ समय बाद ही रीतिकाल के आगमन के चिह्न दिखाई देने लगे थे। राम के मर्यादावादी रूप का सामान्यीकरण करके उसमें भी लौकिक लीलाओं का समावेश कर दिया गया। कृष्ण की प्रेम भक्ति (मूलक) जागृत करने वाली लीलाओं में से कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं को ग्रहण करके उसका अश्लील चित्रण होने लगा था। यह स्थिति रीतिकाल में अपने घोरतम रूप में पहुँच गई थी। इसीलिए कहा गया था “राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है।” रामभक्ति का जो रूप तुलसी ने अंकित किया था, यद्यपि वह धूमिल नहीं हुआ तथापि राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवियों ने श्रृंगारिकता के वातावरण में उसे विस्मृत कर दिया था। इस तरह धीरे-धीरे ई.1680-90 के आसपास भक्तिकाल समाप्त हो गया।
कालान्तर में यद्यपि जनता में भक्तिभाव विद्यमान रहे तथापि न तो इस (तुलसी आदि के समान) को महान विभूति पैदा हो सकी और न कोई बहुत अधिक लोकप्रिय ग्रंथ ही लिखा जा सका।
भक्ति युग का यह आन्दोलन बहुत बड़ा आन्दोलन था एवं ऐसा आन्दोलन भारत ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस साहित्य ने जनता के हृदय में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, जिजीविषा जागृत की, साहस, उल्लास, प्रेम भाव प्रदान किया, अपनी मातृभूमि, इसकी संस्कृति का विराट एवं उत्साहवर्धक चित्र प्रस्तुत किया, लोगों के हृदय में देशप्रेम भी प्रकारंतर से इसी कारण जागृत हुआ।
भक्तियुग में इस तरह मुख्यत: भक्तिपरक साहित्य की रचना हुई परन्तु यह भी पूर्णतया नहीं कहा जा सकता कि किसी अन्य प्रकार का साहित्य उस काल में था ही नहीं। यह अकबर का शासन काल था तथा उसके दरबार में अनेक कवि थे। अब्दुर्रहीम खानखाना आदि की राजप्रसस्तिपरक कुछ कविताएँ मिलती हैं। अकबर ने साहित्य की पारम्परिक धारा को भी प्रोत्साहन दिया था अत: काव्य का वह रूप भी कृपाराम की “हिततरंगिणी” बीरबल के फुटकर दोहों आदि में उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त नीति परक दोहे आदि लिखे गये।
एक और महान कवि आचार्य केशव को शुक्ल जी ने भक्तिकाल के फुटकर कवियों में रखा है। यह कार्य उन्होंने केशव के रचनाकाल के आधार पर किया है। केशव की अलंकार, छंद, रस के लक्षणों – उदाहरणों को प्रस्तुत करने वाली तीन महत्त्वपूर्ण रचनाओं – कविप्रिया, रसिकप्रिया तथा रामचन्द्रिका को भक्ति से भिन्न मान कर भी उन्हें इस युग के फुटकर कवियों में शुक्ल जी ने रखा है परन्तु यह उचित नहीं है। केशव का आचार्यत्त्व पूरे रीतिकाल को गौरव प्रदान करता है। रीति – लक्षण -उदाहरण के निर्धारण की परम्परा भी सर्वप्रथम उन्हीं में दिखाई देती है चाहें रीतिकाल में इस निर्धारण के लिए केशव को रीतिकाल से पृथक करना अनुचित है अत: उन्हें भक्तियुग में रखना उचित नहीं है।
भक्तिकाल और ललित कलाएं
भक्तिकाल में ललित कलाओं का उत्कर्ष दिखाई देता है। श्रीकृष्ण-राधा की विभिन्न लीलाओं के चित्र इस काल में मिलते हैं, कोमल एवं सरस भावों को अभिव्यक्त करने वाली अनेक मूर्त्तियाँ इस काल में मिलती है। मूर्तिकला का बहुत विकास इस युग में बहुत अधिक हुआ था। वास्तुकला, चित्रकला में मुस्लिम (ईरानी) शैली का समन्वय भारतीय शैली में हुआ फलत: मेहराबें, गुम्बद आदि का प्रयोग अधिक दिखाई देने लगा। मध्यकाल में राजस्थानी शैली अधिक लोकप्रिय थी। मानवीय चित्रों के अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्यों का अंकन, दरबारी जीवन के विविध प्रसंग भी भित्ति चित्र इस युग में प्राप्त होते हैं। ’कुतुबमीनार’, ’अढ़ाई दिन का झौंपड़ा’ आदि ऐतिहासिक वास्तुकला के अप्रतिम नमूने हैं।
इस तरह साहित्य के साथ ललित कलाओं का विकास भी बहुत अधिक हुआ था। संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। कृष्णलीलाओं का गायन, साखी, रमैनी, पद को राग निबद्ध करने की जैसी योजना इस काल में है वैसी अन्यत्र प्राप्य नहीं है। सूर और तुलसी साहित्य में अनेक राग-रागनियों का वर्णन आता है।
भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण
प्राचीन काल से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए तीन मार्गों का ज्ञान दिया गया है। यह मार्ग है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। धर्म और ज्ञान का अनुसरण ही भक्ति मार्ग का प्रतीक है। भक्ति का अस्तित्व भारत में प्राचीन काल से ही है। अपने आराध्य देव के प्रति श्रद्धा एवं आस्था का भाव ही भक्ति कहलाता है। वैदिक काल से ही भक्ति का वर्णन अनेक स्थानों पर मिलता है जिसका अर्थ है, भगवान की सेवा करना। भक्ति शब्द का अर्थ है- अनुराग, पूजा, उपासना तथा विभाजन। भक्ति शब्द भज् धातु से बना है जिसका अर्थ है भजना, स्मरण करना या ध्यान करना। श्रद्धा भाव से भगवान की शरण प्राप्त करना, बिना किसी स्वार्थ के भगवान से प्रेम करना और बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करना ही भक्ति कहलाता है।
भारत में भक्ति आंदोलन अत्यधिक प्राचीन है। इसके उद्गम को हम वेदों में देख सकते हैं। हमारे ऋषि-मुनियों ने जिस श्रद्धा और अनुराग के साथ सूर्य, अग्नि, रूद्र, वरुण आदि देवताओं पर ऋचाएं लिखी हैं, वह उनकी भक्ति भावना को ही प्रमाणित करती है। उपनिषद साहित्य में यद्यपि निर्गुण भजन की विवेचना की गई है लेकिन उसमें ज्ञान के साथ है राग तत्व का भी मिश्रण कर दिया गया है। महाभारत तक आते-आते वैष्णव भक्ति का समुचित विकास हो चुका था और विष्णु को भगवान के रूप में प्रतिष्ठा मिल गई थी। श्रीमद्भागवत गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म का सर्वश्रेष्ठ समन्वय देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के उदय के बारे में विचार करने से पहले विद्वानों द्वारा दी गई भक्ति शब्द की परिभाषा पर विचार करना अनिवार्य है जो इस प्रकार है-
नारद भक्ति सूत्र के अनुसार, “पूजादि में अनुराग होना भक्ति है।”
शांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार, “ईश्वर के प्रति अतिशय अनुरक्ति को ही भक्ति कहा गया है।”
श्रीमद् भागवत के अनुसार, ‘मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं है जिसके द्वारा भगवान कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति ऐसी है जिसमें किसी प्रकार की इच्छा ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे।’
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, “श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है।” वह आगे लिखते हैं, “धर्म की रसात्मक अनुभूति ही भक्ति है।”
उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जब धर्म को बिना किसी आडंबर और बुद्धि के सहारे न निभा कर उसमें भावना और हृदय का समावेश कर लिया जाता है तब भक्ति की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की भक्ति के द्वारा भक्त स्वयं भी आनंदित होता है और दूसरों को भी आनंदित करता है।
भक्ति काल का उद्भव और विकास
हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। इसकी समय सीमा संवत् 1375 से संवत् 1700 तक स्वीकार की गई है। भक्ति की इस अविरल परंपरा के उद्भव और विकास को लेकर विद्वानों में अनेक मत प्रचलित हैं। किसी भी युग के उद्भव में तत्कालीन परिस्थितियों अत्यधिक महत्व रखती हैं। भक्ति काल के उदय में भी उस समय की सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति की लहर दक्षिण भारत से विकसित हुई। इसमें आलवार भक्तों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति की इस लहर को रामानंद द्वारा उत्तर भारत में लाया गया।
कबीर के शब्दों में, “भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद”। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, “भक्ति आंदोलन के उदय एवं विकास का श्रेय दक्षिण की आलवार भक्तों को दिया जाना चाहिए। इनकी संख्या बारह मानी गई है। लेकिन यहां पर यह बता देना भी आवश्यक है कि तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण भी भक्ति के उद्भव तथा विकास के लिए उत्तरदाई है। इससे भक्ति भावना का आगमन दक्षिण से हुआ है लेकिन भक्ति का प्रवाह वैदिक युग से चला आ रहा था। फिर यहां राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों ने इसे बल प्रदान किया।”
हिंदी में भक्ति काल का उद्भव कैसे हुआ इस विषय को लेकर तीन प्रकार के मत सामने आते हैं-
प्रथम वर्ग में वो विद्वान आते हैं जो यह मानते हैं कि भक्ति का उद्भव विदेशों में हुआ तथा हिंदी में भक्ति काल ईसाई मत अथवा इस्लाम की देन है।
दूसरा वर्ग उन विद्वानों का है जो व्यक्ति को पराजित निराश हताश जाति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वीकार करते हैं।
तीसरा वर्ग उन विद्वानों का है जो कि भक्ति काल को भारत मे चल रहे धार्मिक आंदोलनों का सहज विकास मानते हैं।
इस प्रकार उत्तर भारत में भक्ति के उद्भव एवं विकास को लेकर विद्वानों ने निम्नलिखित मत दिए हैं-
जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है कि तीसरी चौथी शताब्दी में मद्रास के पास इसाई पादरी उतरे थे उन्हीं के प्रभाव से दक्षिण में भक्ति का प्रचार हुआ।
ताराचंद के अनुसार भक्ति काल का उदय ‘अरबों की देन’ है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृति का परिणाम माना है। वे कहते हैं कि
उस समय मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा से हिंदू धर्म का ह्रास हुआ और उनके भीतर आजादी से संघर्ष करने वाली शक्तियां अत्यंत क्षीण हो गई। जनता निराश और हताश थी उन्हें आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दी। इसलिए उन्होंने स्वयं को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। शुक्ल के शब्दों मे देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू-जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिये वह अवकाश न रह गया। आगे चलकर जब मुसलिम-साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। हताश जाति के लिये भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था?
बाबू गुलाब राय ने भी शुक्ल के मत का ही अनुसरण किया है वह कहते हैं,
“मनोवैज्ञानिक तिथि के अनुसार हार की मनोवृति में दो बातें संभव है या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पढ़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई।”
हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार,
‘मैं तो जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना उचित नहीं है कि इस काल में अधिक अत्याचार हुए। भारत की पराधीनता का इतिहास शोषण एवं अत्याचारों का इतिहास है। भक्तिकाल तो अपेक्षाकृत उदार मुगल बादशाहों का काल रहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह उचित नहीं लगता कि हताश निराश पीड़ित तथा दलित जाति ने ऐसा सुंदर मधुर एवं उत्साहवर्धक साहित्य लिखा होगा। जब गर्दन पर तलवार तनी हो तो मुख से आह या कराह निकलती है सूर और मीरा के गीत नहीं फूटते।
गुलाब राय का यह कहना है कि
अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हिंदू मानस इस ओर झुका जो उचित नहीं है। मुसलमान कवियों ने भी भक्ति साहित्य में योगदान दिया। वे किस के सम्मुख अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे थे? निश्चय ही इस दृष्टि से विश्व का साहित्य निराश हताश पराजित जाति का साहित्य नहीं है। साहित्य की दृष्टि से भी शुक्ल जी का मत ठीक नहीं लगता क्योंकि भक्ति कालीन साहित्य आशा और उत्साह का साहित्य है। इसे साहित्य ने जातीय जीवन को एक नई दिशा दी है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह भी सिद्ध किया कि
भक्ति का उद्भव हेतु एवं पुराणों में ही हो गया था। आलवर संत परंपरा में सगुण और निर्गुण भक्ति विकसित हुई। वहीं से चौदहवीं शताब्दी में रामानंद तथा वल्लभाचार्य जैसे भक्त उत्तर की ओर आने लगे। चैतन्य गोस्वामी के शिष्य रूप गोस्वामी भी काशी में प्रचार के लिए आ गए। महाराष्ट्र में संत परंपरा ज्ञानेश्वर एकनाथ तुकाराम तथा रामदास के माध्यम से चल रही थी। इस प्रकार उत्तर-दक्षिण में एक साथ भक्ति का विकास हो रहा था।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि समग्रतः भक्ति आंदोलन का उदय ग्रियर्सन व ताराचंद के लिए बाहय प्रभाव, शुक्ल के लिए बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया तथा द्विवेदी के लिए भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास था। भक्ति आन्दोलन मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस काल में सामाजिक-धार्मिक सुधारकों की धारा द्वारा समाज विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार-प्रसार किया गया। सिख धर्म के उद्भव में भक्ति आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। भक्ति के उद्भव एवं विकास के समय जो कुछ भी भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति तथा इतिहास को प्राप्त हुआ, वह स्वयं में अद्भुत, अनुपम एवं दुर्लभ है।
अन्ततः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में कह सकते है,
‘समूचे भारतीय इतिहास में यह अपने तरह का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। भक्ति का यह नया इतिहास मनुष्य जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यह लक्ष्य है भगवद्भक्ति, आदर्श है शुद्ध सात्विक जीवन और साधन है भगवान के निर्मल चरित्र और सरस लीलाओं का गान।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने कर्मकांडों से मुक्त जीवन का ऐसा लक्ष्य रखा, जिसमें ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान नहीं था । भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल दिया, जिससे इन समुदायों के मध्य सहिष्णुता और सद्भाव की स्थापना हुई। भक्तिकालीन संतों ने क्षेत्रीय भाषों की उन्नति में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी, पंजाबी, तेलुगू, कन्नड़, बंगला आदि भाषाओं में इन्होंने अपनी भक्तिपरक रचनाएँ कीं। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति-बंधन की जटिलता कुछ हद तक समाप्त हुई। फलस्वरूप दलित व निम्न वर्ग के लोगों में भी आत्मसम्मान की भावना जागी। भक्तिकालीन आंदोलन ने कर्मकांड रहित समतामूलक समाज की स्थपाना के लिये आधार तैयार किया। भक्ति आंदोलन से हिन्दू-मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। भक्तिमार्गी संतों ने समता का प्रचार किया और सभी धर्मों के लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिये प्रयास किये।
भक्ति काल में अनेक उपासना-विधियां, अनेक जातियां, अनेक संप्रदाय सहज भाव से घुलते-मिलते दिखायी देते हैं। एक अलग तरह की संस्कृति जन्म लेती दिखायी देती है, जो अधिक व्यापक, अधिक उदार, अधिक मानवीय है। यह लगभग मान्य सा है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआती धारा द्रविड भाग में उपजी अर्थात् दक्षिण भारत में इसका जन्म हुआ, लेकिन भक्ति आन्दोलन और संस्कृति के रूप में उत्तर भारत में विशेष रूप से फैली है।
बहुत से भक्त कवि कृष्णाश्रय या भगवान की शक्ति और करुणा में विकल्प तलाशते हैं तो कबीर आदि अनेक कवि तत्कालीन चुनौतियों से टकराते भी हैं। यह महत्त्वपूर्ण है कि इस विषम समय में भी भक्तिकाल का कोई कवि मुस्लिम-विद्वेष या साम्प्रदायिकता की अभिव्यक्ति नहीं करता है। कबीर तो हिन्दू-मुसलमान दोनों को राह पर लाने का काम कर ही रहे थे, हिन्दू-तुरक की लड़ाई का वर्णन करने वाले जायसी भी प्रत्यक्ष जीवन में दोनों सम्प्रदायों की एकता दर्शाते हैं।
डॉ. रमेश कुंतल मेघ का यह कथन भी इसकी ताकीद करता है कि हिन्दू-इस्लामी जीवन शैलियों के मिलाप और सर्वधर्म सद्भाव की पहली नींव गुरुनानक और कबीर द्वारा रखी गयी थी। वस्तुतः भक्ति आन्दोलन प्रारम्भ से ही जनता की प्रवृत्तियों का प्रवाह था, अतः उसका चरित्र् समन्वयवादी था। उसमें अनेक पंथ थे, लेकिन वह समग्रतः पंथ-निरपेक्ष था, वह धर्म-केन्द्रित था, लेकिन धर्म निरपेक्ष भी था। लोकमंगल भक्ति-आन्दोलन की केन्द्रीय धुरी है और प्रायः सभी भक्त संत कवि अपने-अपने चिंतन और कविकर्म के माध्यम से न केवल लोक की हित-चिंता में लीन थे, अपितु एक विराट्, उदार, मनुष्यता की पक्षधर संस्कृति को भी पुष्ट कर रहे थे। हर तरह की अमानवीयता का निषेध कर रहे थे, चाहे वह शासकों की क्रूरता हो या धर्माचार्यों का कदाचार हो या रूढ़ियों की जकड़न हो या निरर्थक धार्मिक बाह्याचार हो, ये कवि यथाशक्ति इनका प्रतिवाद करते हैं। इन कवियों ने लोक से वह सब कुछ लिया है जो सहज है, अनिवार्य है, मानव-हित में है और शास्त्र् का वह बहुत कुछ छोड़ दिया है जो रूढ़ियों को प्रश्रय देने वाला है, मनुष्यता का विरोधी है। तुलसी ने रामराज्य और कृष्णभक्त कवियों ने वृन्दावन के रूप में यूटोपिया रचा है, लेकिन यह तत्कालीन यथार्थ से असम्बद्ध नहीं है।
भारतवर्ष में भक्ति साहित्य का आविर्भाव आलवार भक्तों से माना जाता है। माना जाता है कि आलवार (तमिल में आलवार का अर्थ है प्रेम-भक्ति-सागर-मग्न) वैष्णव भक्त ईसा की पाँचवीं से लेकर नवीं सदी तक समय-समय पर हुए हैं और उनके भजन-संगीतों में चार हजार गीतों का संग्रह दिव्य प्रबंधम् बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इस कृति को प्रमुखतः कृष्णकाव्य का आदि रूप कहा जा सकता है। यह ध्यानाकर्षक है कि दाम्पत्य भाव की आराधना की उपस्थिति होते हुए भी आलवार काव्य में राधा का नामोल्लेख नहीं है। लेकिन कृष्ण की प्रियतमा एक प्रधान गोपी नाप्पिन्नाइ का वहाँ कई स्थलों पर उल्लेख है। यह गोपी लक्ष्मी का अवतार मानी गयी है।
डॉ. शशिभूषण दास गुप्त का मानना है – पुराणों में वर्णित कृष्ण की वृन्दावन लीला को लेते समय इस प्रियतमा विशेष की कल्पना को भी भक्त कवियों ने लिया होगा। भक्ति-प्रवाह के उत्तर-भारत में पहुँचने तक हिन्दी भक्तिकाव्य में राधा प्रतिष्ठित हो चुकी थी। आलवार कवियों में संत परकाल, संत रासकोप, संत भक्तिसार, अण्डाल आदि विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। इनके काव्य में उत्तर भारत में आन्दोलन के रूप में रचित भक्ति-साहित्य को अनेक स्तरों पर प्रभावित किया है। लेकिन यह देखने की बात है कि जो साझी संस्कृति हिन्दी के भक्ति-आन्दोलन की विशेषता है वह आलवार-साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होती है। उत्तर-भारत में हिन्दू-मुसलमानों के प्रारम्भिक सांस्कृतिक टकराव के बाद सामंजस्य की दिशाएं खुलती गयी हैं और सकारात्मक सांस्कृतिक आदान-प्रदान का पथ प्रशस्त हुआ है।
डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह अभिमत निर्विवाद कहा जा सकता है –
भक्ति काव्य हिन्दी समाज की उदारतम चेतना का दस्तावेज है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा इस युग के श्रेष्ठ कवि हैं, यह मान्यता सर्वस्वीकृत है। इसका निहितार्थ है कि यहाँ हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्मण-दलित, पुरुष-स्त्री समाज के सभी वर्गों का यह साझा रचना कर्म है।
भक्ति आन्दोलन रामानुज, रामानंद और वल्लभाचार्य आदि आचार्यों से प्रेरित होकर सम्पूर्ण उत्तर भारत में अपनी क्रांतिकारी सुधारवादी चेतना के साथ फूला-फला। गुजरात में नरसी मेहता, महाराष्ट्र में नामदेव, राजस्थान में मीराबाई, पंजाब में गुरुनानक, असम में शंकरदेव, बंगाल में चण्डीदास, उडीसा में सरलदास की रचनाएँ इस विराट् आन्दोलन की पहुँच और पकड़ का प्रमाण देती है। इस्लामी संस्कृति ने इस आन्दोलन को विशेषतः सूफियों के माध्यम से प्रभावित किया जबकि सिद्ध-नाथ बहुत पहले से अपनी वर्णाश्रम विरोधी चिंतना के आधार पर सामाजिक सद्भाव का आह्वान कर रहे थे। इस आन्दोलन में हिन्दुओं के आत्ममंथन के साथ-साथ अनेक मुसलमान इस भक्ति-प्रवाह में अवगाहन करते दिखायी दिये। मुबादशाह कृत राबिस्तां-ए-मजाहिब (रचनाकाल 1645-1653 ई.) में वैरागियों का उल्लेख हुआ है और कबीर को भी वैरागी माना गया है। वैरागियों के बारे में 17वीं शताब्दी का यह साक्ष्य कुछ इस तरह की सूचना देता है –
वैरागी किसी विशेष उपासना पद्धति का पालन नहीं करते। उनका कहना है कि विष्णु का नाम ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है…ये लोग स्वयं को वैष्णव भी कहते हैं और इनका कहना है कि हमारी राह वेद और कुरान की राह से जुदा है। हमें ना हिन्दुओं से वास्ता है ना मुसलमानों से। इनमें मिर्जा सालेह और मिर्जा हैदर जैसे कुलीन मुसलमान भी हैं। दक्खिनी हिन्दी में रचित सूफी काव्य भी भक्तिप्रवाह में हिन्दू-मुसलमानों के सम्मिलन की स्पष्ट गवाही देता है।
सोलहवीं शती के सूफी कवि काजी महमूद बहरी ने दक्खिनी हिन्दी में मन लगन शीर्षक काव्य लिखा है, उसमें सूफी मत को भारतीय चिंतन के निकट लाने का स्पष्ट प्रयास हुआ है। वे सूफी पारिभाषिक शब्दावली को भारतीय चिंतन की शब्दावली के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं –
मैं स्थूल कहूँ बजाय नासूत
सूक्ष्म तो उसे तू समज मलकूत
कारण जबरूत, माह कारन
लाहूत, अपस हिसाब में गिन
मैं जोत को नूर कर कया हूँ
जों जीव को भावै त्यौं भया हूँ।
होर जीव की जा परान बोल्या
इर्फान न बोल ग्यान बोल्या ।
मलकूत, इर्फान की जगह स्थूल और ज्ञान बोलने का आग्रह दुराग्रह नहीं है। वे बताना चाहते हैं कि शब्द अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों चिंतन पद्धतियों का अर्थ और लक्ष्य एक है। जाहिर है, भक्ति आन्दोलन साम्प्रदायिकता से परे सांस्कृतिक आन्दोलन बन चुका था।
भक्तिकाव्य के अध्ययन से यह बात स्पष्ट है कि बाहरी चुनौतियों को स्वीकारने और उनसे जूझने की कोशिश सकारात्मक रही है। आंतरिक चुनौतियों-ब्राह्मणवादी व्यवस्था विशेषतः जातिगत श्रेष्ठता के दंभ, धार्मिक पाखण्ड, ऊँच-नीच का भेदभाव आदि पर प्रहार उनके आत्ममंथन और आत्मालोचन की गवाही देते हैं। खुद को टटोलने और अपनी दुर्बलताओं को चीन्हने की प्रेरणा आंतरिक ही कही जायेगी।
डॉ. भोलाशंकर व्यास के अनुसार आमतौर पर यथास्थितिवादी और रूढ़िवादी समझे जाने वाले सगुण भक्तों और आचार्यों ने भी सामाजिक रूढयों-धार्मिक ब्रह्माचारों की उपेक्षा की है – दक्षिण में रामानुज का प्रपत्तिवाद वस्तुतः उपासना के क्षेत्र् में जात-पाँत की अपेक्षा भगवत्चरणों में सर्वात्मना समर्पण को अधिक महत्त्व देता है और उत्तरी भारत में भी माहव, निम्बार्क, चैतन्य, वल्लभ, हितहरिवंश आदि सगुण भक्त आचार्यों ने भी जात-पाँत की सामाजिक रूढियों को धार्मिक उपासना के क्षेत्र् में झकझोर कर फेंक दिया है।
जाति-पाँति पूछे नहीं कोई/
हरि को भजे सो हरि का होई
इस काव्य के घोषणा पत्र का पहला सिद्धान्त है। इसीलिए सूर जैसे अपने श्याम के रंग में डूबे हुए कवि भी बार-बार कहते हैं
भक्ति में कहाँ जनेऊ- जाति
या
जाति-पाँति कुलकानि न मानत।
न केवल निम्न कही जाने वाली जातियों में जन्मे संत अपितु सवर्ण भक्त भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कटु आलोचक दिखाई देते हैं। हरिराम व्यास लिखते हैं कि
ब्राह्मण के मन भक्ति न आवै/
भूले आप सबनि समझावै।
भक्त कवियों ने जिस संस्कृति का प्रारूप रचा है, उसमें सामंती सत्ता का स्पष्ट तिरस्कार है।
जासुराज मँह प्रजा दुखारी/
सो नृप अवस नरक अधिकारी
इस तिरस्कार का एक छोर है और कुंभनदास का चिंतन संतन कौ कहा सीकरी सौ काम दूसरा छोर है।
भक्ति के अनेकानेक भेदों में दो सर्वमान्य हैं – वैधी भक्ति, परा भक्ति। भक्तिकाल के कवियों ने वैधी या आनुष्ठानिक भक्ति पर जोर नहीं दिया है, भगवान के भाव के भूखे होने का विश्वास उन्हें अधिक है, वहाँ निर्गुण-सगुण का भेद भी सैद्धान्तिक स्तर तक सीमित है –
अगुनहि सगुनहि नहीं कुछ भेदा।
कहीं सगुण पर जोर इसलिए कि निर्गुण सबविधि अगम है। कबीर आदि अवतारवाद के विरोधी हैं, लेकिन पौराणिक संज्ञाएं और मिथक उनके काव्य में बराबर आते हैं, राम हरि, गोविन्द आदि के रूप में। प्रेममार्गी कवियों ने जहाँ हिन्दू आख्यानों को आधार बनाया है, वहीं राम, कृष्ण से जुडे संदर्भ भी उनके प्रेमाख्यानों में जहाँ-तहाँ हैं। कहा जाता है कि अकेले पद्मावत में रामकथा के संदर्भ इतनी बार आये हैं कि उनसे जायसी की स्वतंत्र् रामायण बन सकती है। यह आदान-प्रदान भक्ति आंदोलन की सर्वग्राही और समन्वयवादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप संभव हुआ है।
थोथा अर्थात् अवमूल्यों को उडाकर सार-सार को ग्रहण करने के उदाहरण भक्ति-काव्य में सर्वत्र् द्रष्टव्य हैं।
सम्पूर्ण भक्ति आन्दोलन हमारी साझी विरासत को सहेजने, अंकुठ भाव से अपने विरोधियों से संवाद करने और अवमूल्यों का स्पष्ट तिरस्कार करने का सार्थक सर्जनात्मक अभियान माना जा सकता है। इसमें जब-तब ज्ञान-भक्ति, निर्गुण-सगुण, लोक-शास्त्र्, ब्राह्मण-शूद्र, हिन्दू-मुसलमान, शैव-वैष्णव आदि उलझते हैं, सुलझते हैं और अंततः मनुष्यता के पक्ष में कुछ मूल्यों को सौंप जाते हैं। प्रायः कबीर आदि संत कवियों को सूर-तुलसी की तुलना में कहीं अधिक प्रासंगिक माना जाता है और उन्हें दूसरी परम्परा से संबंधित किया जाता है।
ऐसा होता तो क्या कोई कृष्णभक्त कवि लिखता – कलि में साँचो भक्त कबीर। वस्तुतः कबीर हो या तुलसी या सूर या जायसी में एक ही विराट् आन्दोलन – भक्ति आन्दोलन के अंग थे। दिखायी देने वाले मतभेद बाहरी हैं, उनकी रचनाशीलता की अन्तरात्मा एक जैसी है। यही कारण है कि देश का जनमानस, जितना तुलसी आदि सगुणोपासकों को अपने निकट पाता है, उतने ही उसे कबीर, रैदास भी अपने लगते हैं। जनश्रुति है कि रैदास मीरा के गुरु थे। इससे भी स्पष्ट है कि भक्त के स्तर पर अगुन और सगुन का कोई भेद नहीं बचा था।
आज भक्ति साहित्य को कभी दलित विमर्श के निकष पर कसा जाता है तो कभी नारी-विमर्श के आधार पर उसकी प्रासंगिकता आँकी जाती है। वस्तुतः भक्ति अपने आप में एक विराट् विमर्श है। इसका पहला विचार सूत्र् है —
जाति पाँति पूछे नहिं कोई/हरि को भजे सो हरि का होई।
इसका दूसरा सूत्र् है
– अरे इन दोउन राह न पाई। मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी
इसकी संवेदना का एक छोर है और प्रेम के आगे सारे विधि- नियम, वर्णाश्रम शिथिल हो जाते हैं। चौथे पुरुषार्थ मोक्ष का इसमें स्पष्ट तिरस्कार है।
गति न चहऊँ निरवान और मुक्ति आनिमंदे में घेली आदि उद्गार इस संदर्भ में ध्यानाकर्षक हैं। धर्म की नयी और सार्वकालिक व्याख्या इसी विमर्श का निचोड है – परहित सरिस धर्म नहिं भाई।
विराट् भक्ति-आन्दोलन की तुलना केवल एक और जन-आंदोलन भारत के स्वाधीनता संग्राम से की जा सकती है। दोनों ही विराट् जनहित में अवमूल्यों के प्रति एक संयुक्त सांस्कृतिक प्रतिवाद दर्ज कराते हैं। स्वाधीनता-आंदोलन के दौरान तुलसीदास की नारी से संबंधित एक उक्ति पराधीनता के विरुद्ध शंखनाद बन गयी थी – पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं। नरसी मेहता का वैष्णव जन तो तैने कहिए… गाँधी जी की प्रार्थना सभाओं में गाया ही जाता था और यह भी परहित सरिस धर्म नहि भाई की मूल भावना का समर्थन था।
डॉ. मैनेजर पाण्डेय का यह कथन सही है कि गाँधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा मीराबाई से मिली और रामराज्य की कल्पना तुलसीदास से। उनका चरखा कबीर का है और पराई पीर अनुभव करने वाली संवेदनशीलता नरसी मेहता की। डॉ. पाण्डेय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गाँधी के हृदय के विवेक का मूल स्रोत भक्ति-काव्य की संवेदना उसकी लोकधर्मिता और मूलगामी मानवीयता है न कि तोलोस्तोय और रस्किन के विचार ….। आज भी साम्प्रदायिक विद्वेष, अमानवीयकरण आदि अवमूल्यों के वर्चस्व के दौर में यह संवेदना, संस्कृति और मानवीयता बहुत काम की है।
इस तरह देखें तो संतसाहित्य का अर्थ है- वह धार्मिक साहित्य जो निर्गुणिए भक्तों द्वारा रचा जाए। यह आवश्यक नहीं कि सन्त उसे ही कहा जाए जो निर्गुण उपासक हो। इसके अंतर्गत लोकमंगलविधायी सभी सगुण-निर्गुण आ जाते हैं, किंतु आधुनिक ने निर्गुणिए भक्तों को ही “संत” की अभिधा दे दी और अब यह शब्द उसी वर्ग में चल पड़ा है।
“संत” शब्द संस्कृत “सत्” के प्रथमा का बहुवचनान्त रूप है, जिसका अर्थ होता है सज्जन और धार्मिक व्यक्ति। हिन्दी में साधु/सुधारक के लिए यह शब्द व्यवहार में आया। कबीर, रविदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास आदि पुराने भक्तों ने इस शब्द का व्यवहार साधु और परोपकारी, पुरुष के अर्थ में बहुलांश: किया है और उसके लक्षण भी दिए हैं।
लोकोपकारी संत के लिए यह आवश्यक नहीं कि यह शास्त्रज्ञ तथा भाषाविद् हो। उसका लोकहितकर कार्य ही उसके संतत्व का मानदंड होता है। हिंदी साहित्यकारों में जो “निर्गुणिए संत” हुए उनमें अधिकांश अनपढ़ किंवा अल्पशिक्षित ही थे। शास्त्रीय ज्ञान का आधार न होने के कारण ऐसे लोग अपने अनुभव की ही बातें कहने को बाध्य थे। अत: इनके सीमित अनुभव में बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं, जो शास्त्रों के प्रतिकूल ठहरें। अल्पशिक्षित होने के कारण इन संतों ने विषय को ही महत्व दिया है, भाषा को नहीं। इनकी भाषा प्राय: अनगढ़ और पंचरंगी हो गई है। काव्य में भावों की प्रधानता को यदि महत्व दिया जाए तो सच्ची और खरी अनुभूतियों की सहज एवं साधारणोकृत अभिव्यक्ति के कारण इन संतों में कइयों की बहुवेरी रचनाएँ उत्तम कोटि के काव्य में स्थान पाने की अधिकारिणी मानी जा सकती है। परंपरापोषित प्रत्येक दान का आँख मूँदकर वे समर्थन नहीं करते। इनके चिंतन का आकार सर्वमानववाद है। ये मानव मानव में किसी प्रकार का अंतर नहीं मानते। इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुलविशेष के कारण किसी प्रकार वैशिष्ट्य लिए हुए उत्पन्न नहीं होता। इनकी दृष्टि में वैशिष्ट्य दो बातों को लेकर मानना चाहिए : अभिमानत्यागपूर्वक परोपकार या लोकसेवा तथा ईश्वरभक्ति। इस प्रकार स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में इन संतों ने एक प्रकार की वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।
निर्गुणिए संतों की वाणी मानवकल्याण की दृष्टि से जिस प्रकार के धार्मिक विचारों एवं अनुभूतियों का प्रकाशन करती हैं वैसे विचारों एवं अनुभतियों को पुरानी हिंदी में बहुत पहले से स्थान मिलने लगा था। विक्रम की नवीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों ने जो रचनाएँ प्रस्तुत कीं उनमें वज्रयान तथा सहजयान संबंधी सांप्रदायिक विचारों एवं साधनाओं के उपन्यसन के साथ-साथ अन्य संप्रदाय के विचारों का प्रत्याख्यान बराबर मिलता है। उसके अनंतर नाथपंथी योगियों तथा जैन मुनियों की जो बानियाँ मिलती हैं, उनमें भी यही भावना काम करती दिखाई पड़ती है। बौद्धों में परमात्मा या ईश्वर को स्थान प्राप्त न था, नाथपंथियों ने अपने वचनों में ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा की। इन सभी रचनाओं में नीति को प्रमुख स्थान प्राप्त है। ये जगह-जगह लोक को उपदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। पुरानी हिंदी के बाद जब हिंदी का विकास हुआ तब उसपर भी पूर्ववर्ती साहित्य का प्रभाव अनिवार्यत: पड़ा। इसीलिए हिंदी के आदिकाल में दोहों में जो रचनाएँ मिलती हैं उनमें से अधिकांश उपदेशपरक एवं नीतिपरक हैं। उन दोहों में कतिपय ऐसे भी है जिनमें काव्य की आत्मा झलकती सी दिखाई पड़ जाती है। किंतु इतने से ही उसे काव्य नहीं कहा जा सकता।
पंद्रहवी शती विक्रमी के उत्तरार्ध से संतपरंपरा का उद्भव मानना चाहिए। इन संतों की बानियों में विचारस्वातंत्र्य का स्वर प्रमुख रहा वैष्णव धर्म के प्रधान आचार्य रामानुज, निंवार्क तथा मध्व विक्रम की बारहवीं एवं तेरहवीं शती में हुए। इनके माध्यम से भक्ति की एक वेगवती धारा का उद्भव हुआ। इन आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी पर जो भाष्य प्रस्तुत किए, भक्ति के विकास में उनका प्रमुख योग है। गोरखनाथ से चमत्कारप्रधान योगमार्ग के प्रचार से भक्ति के मार्ग में कुछ बाधा अवश्य उपस्थित हुई थी, जिसकी ओर गोस्वामी तुलसीदास ने संकेत भी किया है :
गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग।
तथापि वह उत्तरोत्तर विकसित होती गई। उसी के परिणामस्वरूप उत्कल में संत जयदेव, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत [[नामदेव तथा ज्ञानेदव, पश्चिम में संत सधना तथा बेनी और कश्मीर में संत लालदेव का उद्भव हुआ। इन संतों के बाद प्रसिद्ध संत रामानंद का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी शिक्षाओं का जनसमाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। यह इतिहाससिद्ध सत्य है कि जब किसी विकसित विचारधारा का प्रवाह अवरुद्ध करके एक दूसरी विचारधारा का समर्थन एवं प्रचार किया जाता है तब उसके सिद्धांतों के युक्तियुक्त खंडन के साथ उसकी कतिपय लोकप्रिय एवं लोकोपयोगी विशेषताओं को आत्मीय भी बना लिया जाता है। जगद्गुरु शंकर, राघवानंद, रामानुज, रामानंद आदि सबकी दृष्टि यही रही है। श्रीसंप्रदाय पर नाथपंथ का प्रभाव पड़ चुका था, वह उदारतावादी हो गया था। व्यापक लोकदर्शन के फलस्वरूप स्वामी रामानंद की दृष्टि और भी उदार हो गई थी। इसीलिए उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शिष्यों में जुलाहे, रैदास, नाई, डोम आदि सभी का समावेश देखा जाता है। इस काल में जो सत्यभिनिवेशी भक्त या साधु हुए उन्होंने सत् के ग्रहणपूर्वक असत् पर निर्गम प्रहार भी किए। प्राचीन काल के धर्म की जो प्रतीक प्रधान पद्धति चली आ रही थी, सामान्य जनता को, उसका बोध न होने के कारण, कबीर जैसे संतों के व्यंग्यप्रधान प्रत्यक्षपरक वाग्बाण आकर्षक प्रतीत हुए। इन संतों में बहुतों ने अपने सत्कर्तव्य की इतिश्री अपने नाम से एक नया “पंथ” निकालने में समझी। उनकी सामूहिक मानवतावादी दृष्टि संकीर्णता के घेरे में जा पड़ी। इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी से उन्नीसवीं शताब्दी तक नाना पंथ एक के बाद एक अस्तित्व में आते गए। सिक्खों के आदि युग नानकदेव ने (सं. 1526-95) नानकपंथ, दादू दयाल ने (1610 1660) दादूपंथ, कबीरदास ने कबीरपंथ, बावरी ने बावरीपंथ, हरिदास (16 वीं शती उत्तरार्ध) ने निरंजनी संप्रदाय और मलूकदास ने मलूकपंथ को जन्म दिया। आगे चलकर बाबालालजी संप्रदाय, धानी संप्रदाय, साथ संप्रदाय, धरनीश्वरी संप्रदाय, दरियादासी संप्रदाय, दरियापंथ, शिवनारायणी संप्रदाय, गरीबपंथ, रामसनेही संप्रदाय आदि नाना प्रकार के पंथों एवं संप्रदायों के निर्माण का श्रेय उन संतों को है जिन्होंने सत्यदर्शन एवं लोकोपकार का व्रत ले रखा था और बाद में संकीर्णता को गले लगाया। जो संत निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हुए राम, कृष्ण आदि को साधारण मनुष्य के रूप में देखने के आग्रही थे वे स्वयं ही अपने आपको राम, कृष्ण की भाँति पुजाने लगे। संप्रदायपोषकों ने अपने आदि गुरु को ईश्वर या परमात्मा सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार की कल्पित आख्यायिकाएँ गढ़ डालीं। यही कारण है कि उन सभी निर्गुणिए संतों के वृत्त अपने पंथ या संप्रदाय की पिटारी में ही बंद होकर रह गए।
इधर साहित्य में जब से शोधकार्य ने बल पाया है तब से साहित्यग्रंथों के कतिपय पृष्ठों में उनकी चर्चा हो जाती है, जनसामान्य से उनका कोई संपर्क नहीं रह गया है। इन संप्रदायों में दो एक संप्रदाय ऐसे भी देख पड़े, जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति को गौण किंतु कर्म को प्रधानता दी। सत्तनामी संप्रदायवालों ने मुगल सम्राट् औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का झंडा ऊपर लहराया था (सवत 1729 विक्रमी)। नानकपंथ के नवें गुरु श्री गोविंद सिंह ने अपने संप्रदाय को सेना के रूप में परिणम कर दिया था। इसी संतपरंपरा में आगे चलकर राधास्वामी संप्रदाय (19वीं शती) अस्तित्व में आया। यह संतपरंपरा राजा राममोहन राय (ब्रह्मसमाज, 1835-90), स्वामी दयानन्द सरस्वती (संवत् 1881-1941 विक्रमी, आर्यसमाज), स्वामी रामतीर्थ (सं. 1930-63), तक चली आई है। महात्मा गांधी को इस परंपरा की अंतिम कड़ी कहा जा सकता है।
जैसा पहले कहा जा चुका है, इन संप्रदायों और पंथों के बहुसंख्यक आदि गुरु अशिक्षित ही थे। अत: वे मौखिक रूप में अपने विचारों और भावों को प्रकट किया करते थे। शिष्यमंडल उन्हें याद कर लिया करता था। आगे चलकर उन्हीं उपदेशात्मक कथनों को शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध कर लिया गया और वही उनका धर्मग्रंथ हो गया। इन कथनों एवं वचनों के संग्रह में कहीं कहीं उत्तम और सामान्य काव्य की बानगी भी मिल जाती है। अत: इन पद्यकार संतों में कतिपय ऐसे संत भी हैं जो मुख्यत: संत होते हुए भी गौणत: कवि भी इसमें कइयों ने अपनी शास्त्रीय शिक्षा के अभाव को बहुश्रुतता द्वारा दूर करने का प्रयास अवश्य किया है, यह भी दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नहीं। इनमें बहुतों का साहित्य के स्वरूप से परिचय तक नहीं था किंतु उनकी अनुभति की तीव्रता किसी भी भावुक के चित्त को प्राकृष्ट कर सती है। ऐसे संतों में कबीर का स्थान प्रमुख है। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों की धार्मिक परंपराओं एवं रूढ़िगत कतिपय मान्यताओं पर, बिना दूरदर्शितापूर्वक विचार कि, उन्होंने जो व्यंग्यात्मक प्रहार किए और अपने को सभी ऋषियों मुनियों से आचारवान् एवं सच्चरित्र घोषित किया, उसके प्रभाव से समाज का निम्नवर्ग अप्रभावित न रह सका एवं आधुनिक विदेशी सभ्यता में दीक्षित एवं भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति से परांमुख कतिपय जनों को उसमें सच्ची मानवता का संदेश सुनने को मिला। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्मसमाजी विचारों से मेल खाने के कारण कबीर की बानियों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया और उससे आजीवन प्रभावित भी रहे। कबीर की रचना मुख्यत: साखियों और पर्दों में हुई हैं। इनमें उनकी स्वानुभूतियाँ तीव्र रूप में सामाने आई हैं। संतपरंपरा में हिंदी के पहले संतसाहित्यभ्रष्टा जयदेव हैं। ये गीतगोविंदकार जयदेव से भिन्न हैं। सधना, त्रिलोचन, नामदेव, सेन भाई, रैदास, पीपा, धन्ना, नानकदेव, अमरदास, धर्मदास, दादूदयाल, बषना जी, बावरी साहिबा, गरीबदास, सुंदरदास, दरियादास, दरिया साहब, सहजो बाई आदि इस परंपरा के प्रमुख संत हैं।
संतवाणी की विशेषता यही है कि सर्वत्र मानवतावाद का समर्थन करती है।
भक्ति आंदोलन में नयनार को शैववाद कहा जाता है। सातवीं से नौवीं शताब्दी में नयनारों (शिव को समर्पित संत) और अलवर (विष्णु को समर्पित संत) के नेतृत्व में नई धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। वे सभी जातियों से आए थे, जिनमें पुलाईयर और पनार जैसे ‘अछूत’ माने गए थे। वे बौद्धों और जैन के तीव्र आलोचक थे और मोक्ष के मार्ग के रूप में शिव या विष्णु के प्रबल प्रेम का प्रचार करते थे। उन्होंने प्रेम और वीरता के आदर्शों को आकर्षित किया जैसा कि संगम साहित्य (तमिल साहित्य का सबसे पहला उदाहरण, सामान्य युग की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान रचा गया था) में पाया जाता है और उन्हें भक्ति के मूल्यों के साथ मिश्रित किया।
इस दौरान 63 नयनार थे, उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे अप्पार, सांभरदार, सुंदरार और मणिक्कवासागर।
12 अलवर थे, जो समान रूप से भिन्न पृष्ठभूमि से आए थे, सबसे प्रसिद्ध पेरियालवर, उनकी बेटी अंदल, टोंडारादिपोदी अलवर और नम्मलवार। उनके गीत दिव्य प्रभुधाम में संकलित किए गए थे। अलवर विष्णु के भक्त हैं। दूसरा शब्द शिव भक्तों के लिए होगा।
यहां बोधिसत्व भी हैं, उस व्यक्ति को बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है, जो बुद्ध बनने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर है। वहीं सूफी, वली, दरवेश और फ़कीर शब्द मुस्लिम संतों के लिए उपयोग किए जाते हैं। वली एक सूफी थे, जिन्होंने अल्लाह से निकटता का दावा किया था। संत वे व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने तपस्वी अभ्यास, चिंतन, त्याग और आत्म-अस्वीकार के माध्यम से अपने सहज ज्ञान युक्त संकायों के विकास को प्राप्त करने का प्रयास किया।
इस तरह मध्य काल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार तथा नयनार संतों द्वारा की गई। बारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था- हिन्दू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिन्दू धर्म में समन्वय स्थापित करना। अपने उद्देश्यों में यह आंदोलन काफी हद तक सफल रहा।